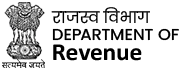- अपीलीय अधिकरण को मूल रूप से तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 (सफेमा) के तहत 1977 में 'सम्पह्त संपत्ति अपीलीय अधिकरण' (एटीपीएफ) के रूप में गठित किया गया था। इस प्रकार, यह देश के शुरुआती न्यायाधिकरणों में से एक है। सफेमा समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, तत्कालीन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (एफइआरए) और एफइआरए, 1973 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों और कोफेपोसा के तहत हिरासत में लिए गए लोगों पर लागू होता है, जिनके हिरासत आदेशों को अधिनियम की धारा 2 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार न तो सरकार द्वारा रद्द किया गया था और न ही सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों द्वारा ही रद्द किया गया था। यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए निर्देशित है। ऐसे व्यक्तियों के रिश्तेदारों और सहयोगियों को भी अधिनियम के दायरे में लाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन दोषियों/बंदियों पर यह अधिनियम लागू होता है, उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां, जो उनके रिश्तेदारों या सहयोगियों के नाम पर हैं, वे भी इस दायरे से बाहर न निकल सकें। इसी तरह, किसी भी संपत्ति के धारक जो पहले किसी भी समय ऐसे व्यक्ति के पास थी, को भी प्रावधानों के दायरे में लाया गया है, जब तक कि ऐसे धारक यह साबित न कर सके कि वे पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावनापूर्वक हस्तांतरित किए गए हैं।
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) 1985 में अधिनियमित किया गया था, क्योंकि स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पर व्यापक कानून के अधिनियमन की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई थी, जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वापक औषधियों से संबंधित मौजूदा कानूनों को समेकित और संशोधित करेगा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर मौजूदा नियंत्रण को मजबूत करेगा, विशेष रूप से तस्करी के अपराधों के लिए दंड को पर्याप्त रूप से बढ़ाएगा, मन:प्रभावी पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए प्रावधान करेगा और स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करेगा, जिसका भारत एक पक्ष बन गया है।
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए 1989 में एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन किया गया था। अधिनियम में एक नया अध्याय-V क जोड़ा गया था, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उसमें इस्तेमाल की गई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को अधिग्रहण करने, फ्रीज करने और जब्त करने का प्रावधान था। नए अध्याय के प्रावधान कमोवेश सफेमा के प्रावधानों के अनुरूप थे। इसके परिणामस्वरूप, एटीएफपी ने एऩडीपीएस अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के तहत मामलों की सुनवाई भी शुरू कर दी।
- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया था क्योंकि यह पाया गया कि धन शोधन और संबंधित गतिविधियों को रोकने के लिए व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता थी, जो न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करते थे। धन शोधन निवारण विधेयक, 1998 नामक एक व्यापक विधेयक 4 अगस्त 1998 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 4 मार्च, 1999 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद विधेयक को 17 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के रूप में क़ानून की किताब में आया। इस अधिनियम की धारा 25 में अधिनियम के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकरणों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपीलीय अधिकरण स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार को अधिदेश दिया गया था।
- वित्त अधिनियम 2016, जिसमें विभिन्न अधिनियमों के तहत गठित कुछ मौजूदा न्यायाधिकरणों के विलय के प्रावधान शामिल थे, ने अन्य बातों के साथ-साथ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 25 को एक नई धारा 25 से प्रतिस्थापित किया, जिसमें यह प्रावधान है कि सफेमा के तहत गठित अपीलीय अधिकरण दिनांक 01.06.2016 से अधिनियम के तहत अधिकरण और अन्य प्राधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए एक अपीलीय अधिकरण होगा। उसी वित्त अधिनियम ने इस अपीलीय अधिकरण का नाम भी “सम्पह्त संपत्ति अपीलीय अधिकरण” से संशोधित कर “अपीलीय अधिकरण” कर दिया।
- उसी वर्ष, अर्थात् वर्ष 2016 में, बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था, जिसे उसी संशोधन अधिनियम द्वारा 'बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (पीबीपीटीए)' नाम दिया गया था, दिनांक 25.10.2016 को एक अधिसूचना जारी की गई थी कि पीएमएलए की धारा 25 के तहत स्थापित अपीलीय अधिकरण संशोधित बेनामी अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकरण के कार्यों का निर्वहन करेगा।
- वित्त अधिनियम, 2017 के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 18 के अंतर्गत गठित विदेशी मुद्रा अपीलीय अधिकरण (एटीएफई) को भी सफेमा के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण में विलय कर दिया गया।
- ऊपर वर्णित घटनाओं के अनुक्रम के परिणामस्वरूप, अपीलीय अधिकरण, जैसा कि यह वर्तमान में मौजूद है, सफेमा, पीएमएलए और फेमा के तहत स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरणों का समूह है। यह वर्तमान में पाँच केंद्रीय अधिनियमों, अर्थात् सफेमा (1976), एनडीपीएस अधिनियम (1985), पीएमएलए (2002), बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम (पीबीपीटीए) (1988) जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया है, और फेमा (1999) के तहत दाखिल होने वाली अपीलों की सुनवाई करता है। यह अधिकरण सफेमा/एनडीपीएस अधिनियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी, पीएमएलए के तहत न्यायनिर्णयन और अन्य प्राधिकारियों और बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत आयकर विभाग द्वारा पारित कुर्की/जब्ती आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों और संबद्ध याचिकाओं पर निर्णय लेता है। यह वित्तीय आसूचना एकक, भारत (एफआईयू-भारत) द्वारा पारित जुर्माना लगाने के आदेशों और फेमा के तहत अन्य प्राधिकरणों द्वारा जुर्माना लगाने के आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों पर भी निर्णय देता है।
- अपीलीय अधिकरण एक राष्ट्रीय अधिकरण है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली के चौथे तल, 'ए' और 'सी' विंग से कार्य करता है। वर्तमान में, इसकी कोई अन्य स्थायी पीठ नहीं है। अपीलीय अधिकरण में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं।
- अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार, कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो या रहा हो, और वह सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत सरकार के अपर सचिव के पद या किसी समकक्ष या उच्च पद पर न रहा हो और उसने तीन वर्षों तक न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या न्यायनिर्णयन संबंधी कार्य न किया हो।
- जबकि पीएमएलए, पीबीपीटीए और फेमा के तहत अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील संबंधित अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय में की जा सकती है, वहीं साफेमा और एनडीपीएस अधिनियमों में इस अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने का प्रावधान नहीं है।
Primary Color
Default
Red
Blue
Green

अपीलीय अधिकरण (सफेमा)